
हमारे दरकते रिश्ते और सिमटते हुए रास्ते Publish Date : 18/05/2024
हमारे दरकते रिश्ते और सिमटते हुए रास्ते
डॉ0 आर. एस. सेंगर

भावनाएं शनैः शनैः सूखती जाती हैं, तो आंखें भी अहसास से खाली होती जाती हैं, संवेदनाएं शून्य होती जाती हैं। दिल में जज्बातों का ज्वार नहीं उमड़ता, माहौल में अजनबीपन घर कर जाता है, ऐसी स्थिति में हवा भी हौले-हौले परायी ही लगने लगती है। जाने कब मन की मचलती मछली को कोई विष वाक्य का तीर भेद जाता है, मर जाता है तो मन ऐसा हो जाता है, कतरा-ए- खूं नहीं निकलता, पर दिल चाक चाक हो जाता है और कुछ भी पता नहीं चलता।
रिश्तों को सहेजने, संवारने, सींचने का दायित्व बुजुर्ग पीढ़ी पर जितना है, उतना ही सहलाने का महती भार युवा पीढ़ी पर भी है। कोई भी वृक्ष अपनी कोपल, अपनी पौध या अपने ही वंश के बीज को दरकार रोशनी, पानी, हवा, खाद में साझेदारी या बंटवारे के बारे में नहीं सोचता, वरन् अपने हिस्से की चीजें लुटाता ही है और समय-असमय, होनी- अनहोनी के अंधड़ में इन कोंपलों पर युवा पौध पर सुरक्षा की छतरी भी लगा देता है। परंतु पौधे और एक वृक्ष का आकार ग्रहण करती यह युवा पीढ़ी सोचती है कि हमारे अधिकार की रोशनी पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए।
सोचते हैं कि हमारा ‘स्पेस’ कुछ कम है, परन्तु इके सम्बन्ध में विचारणीय बात तो यह कि ‘आसमान को मुट्ठी’ में करने वाली पीढ़ी ने ‘फेस’ ही कितना किया है, इसकी अपेक्षा यह पीढ़ी एक गैर जरूरी ‘रेस’ में अवश्य ही कूद पड़ी है। जब उन्हें यहां नहीं कुछ हासिल होता है तो फिर उन्हें ‘ठेस’ ही लगती है। नहीं कुछ पाने का आक्रोश, दूसरों को मिली उपलब्धियों पर स्वयं के मन में व्यर्थ मलाल होना। चित्त में, व्यवहार में ये मलाल उद्वेग, आक्रोश में रूपांतरित होता है जो अनावश्यक ही होता है। पर युवा पीढ़ी अपने सपनों, आकांक्षाओं को पूरा करने की मृग मरीचिका में रिश्तों के सीनों पर पैर रखकर आगे तो बढ़ जाती है पर पहुँचती कहीं भी नही है और यह कांच से संबंध धीरे-धीरे दरकते रहते हैं और बाद में किरचे किरचे ही रह जाते हैं।

एक विचित्र विरोधाभास यह है कि युवा और अधेड़ होती पीढ़ी को पंख चाहिए, परवाज ( उड़ान) चाहिए, बस परिवार ही नहीं चाहिए। समृद्धि चाहिए, परन्तु संबंधी नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, परन्तु दुनियादारी नहीं चाहिए। सगे-संबंधी यानी कि माता-पिता, सास-ससुर मिल जाएं तो यह ऑफर स्कीम में तो उनसे सर्विस (आफ्टर डिलीवरी) भी पूरी ही मिलनी चाहिए, परन्तु यदि जरूरत पड़े तो स्वयं की सर्विस और उसका मैंटेनेंस फ्री होना चाहिए। परिवार के अन्य रिश्तों की खरपतवार को तो होना ही नहीं चाहिए, हालांकि इसमें कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं।
आज बहू, अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, पति की आमदनी इतनी नहीं कि भाई का घर छोड़ अपना डेरा बसाए, जीवन के अक्टूबर-नवंबर में चल रहे बुजुगों की सेहत ऐसी नहीं कि स्वयं अपनी देख-रेख और निर्वाह कर सकें। ऐसी इकाइयों के घर के प्रथम परिवार यानी कि मियां-बीबी और बच्चे, हद से हद अपरिहार्य बुजुर्ग रहते हैं। पर पारंपरिक संयुक्त परिवार की कबीलाई संरचना, जिसमें देवर- जेठ- ककेरे चचेरे रिश्तों की खरपतवार तो एकदम ही नागवार होती है।
हम संवेदनाओं के धरातल पर ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति में जितनी ऋतुएं हैं, उतने ही उतार-चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं। जेठ का ताप है, तो वहीं सावन की शीतलता भी है। बसंत बहार है तो चैत की पतझड़ भी है। इधर परस्पर व्यवहार में कुछ लोप हुआ है तो वह है माधुर्य के रस का। अब संबंधों की साज से संगीत तो निकलता ही नहीं है, अलबत्ता तार को खींचने, मरोड़ने, तोड़ने की तिकड़म होती है। मन का अंतराल पीढ़ियों से चढ़ने वाली सीढ़ियां छोड़ता है, तो यह अंतर अपनी सतह पर आ जाता है।
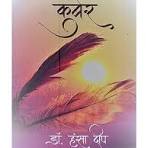
आचरण में शिष्टता, व्यवहार की शालीनता, कर्म की शुचिता के स्थान पर अब रिश्तों में संदेह के बीज बोना, संबंधों में शिथिलता होना, भावों में शुष्कता का आना, आज के इस मोबाइल कनेक्टिंग युग में आम हो गया है और जब चलन में ये खोटे सिक्के भारी मात्रा में हो तो इस अंधड़ में खरे सिक्कों के गुम होने की, डिसकनेक्ट होने की आशंका बेवजह ही नहीं होती। महानगरों की मायावी चकाचौंध में नजरें एक जगह टिकती नहीं, हर वस्तु को पाने की ललक में पैर जमीं पर पड़ते ही नहीं।
स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिये बच्चों का अपना शहर, नगर, गांव छूटता है, और छूट जाता है घर भी और छिटकते जाते रिश्ते। बहरहाल ये तो वक्त का तकाजा है उनकी तरक्की के लिये। वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते थे- रोटी केवल घर पर ही मिलती है लेकिन उसे कमाने परदेश जाना ही पड़ता है। इन दिनों युवा पीढ़ी के परस्पर रिश्तों में गौत्र, कुटुंब, जाति समाज के मुद्दे उभरते हैं। पर वैश्विक ग्राम के रूप में तेजी से बदलती इस दुनिया में मेरा मानना है कि गौत्र या वर्ण केवल दो-चार ही शेष रह गए हैं।
पूर्व में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे और अब भारतीय संदर्भ में और वर्तमान समय में ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम आदि में रूपांतरित हो गए हैं जिनमें विवाह मेल या रोटी-बेटी के संबंध तो हो सकते हैं। उपभोक्तावादी मानसिकता, प्रवृत्ति से जूझ रहे शाख से टूट से रहे ये पत्ते, अब कब समझेंगे ? हमारी पीढ़ी पश्चिम संस्कृति, सभ्यता, सोच से भले ही एक-दो-पीढ़ी पीछे चल रहे हों पर ये परिवर्तन वहां भी आज से एक-दो पीढ़ी पहले शुरू हो गया था। इसलिए सिमटते संबंधों का शिलालेख तो अब लिखा ही जा चुका है।

लेखकः प्रोफेसर आर. एस. सेंगर, निदेशक प्रशिक्षण, सेवायोजन एवं विभागाध्यक्ष प्लांट बायोटेक्नोलॉजी संभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।


