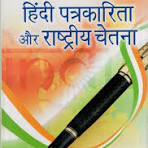
हिन्दी पत्रकारिता में सवाल दर सवाल Publish Date : 27/06/2025
हिन्दी पत्रकारिता में सवाल दर सवाल
प्रोफेसर आर. एस. सेंगर
मिशन के साथ शुरू हिन्दी पत्रकारिता में खबर और विज्ञापन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। पेड न्यूज ने भाषाई अखबारों की छवि को आहत किया है। सरकारें पत्रकारों पर जब चाहे शिकंजा इस नाते कसती रहती हैं कि पत्रकारों को नियंत्रित करने के लिए 14 विभिन्न कानूनों का जाल है। हिन्दी पत्रकारिता का सफर करीब 200 सालों का हो गया है। अब सूचना और संचार क्रांति के इस दौर को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया आयाम देने जा रहा है।

30 मई, 1826 को कलकत्ता में अहिन्दी भाषियों के बीच से हिन्दी का पहला अखबार 'उदन्त मार्तण्ड' पं. जुगल किशोर और सुकुल जी कुशल के संपादन में साप्ताहिक रूप में निकला तो कोई खास हलचल नहीं हुई। इसके पीछे कोई बड़ी संख्या वा पूंजी नहीं थी। पहले अंक की 500 प्रतियां ही छपों और 79 अंक निकाल कर तंगहाली में 4 दिसम्बर, 1826 को यह अखबार अस्ताचल को चला गया। विपरीत परिस्थितियों में यथासंभव अखबार चला, लेकिन इतिहास में यह अखबार और सुकुल जी दोनों अमर हो गए।
आपातकाल के दौरान जब इसके प्रकाशन का 150 साल हो रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में विख्यात हिन्दी सेवी ठाकुर प्रसाद सिंह के प्रयासों से हिन्दी पत्रकारों और लेखकों का जमावड़ा हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। 30 मई, 1977 के बाद से यह दिवस मनाया जाना आरंभ हुआ। आज देश में 350 से ज्यादा न्यूज चैनलों में अधिकतर हिन्दी के हैं। पंजीकृत पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 1,44,520 है, जिनमें अधिकतर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के हैं। कोरोना महामारी में अखबारों का प्रसार गिरा, तमाम पत्र-पत्रिकाएं बंद हो गईं। बावजूद हिन्दी मीडिया ताकतवर होती जा रही है।
बीती दो सदी के बीच हिन्दी पत्रकारिता ने लंबा सफर तय किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माधव राव सप्रे, गणेशशंकर विद्यार्थी, मुंशी प्रमेचंद, शिवपूजन सहाय से लेकर इसको शक्ति देने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। हिन्दी की तमाम पत्र-पत्रिकाएं भोपाल में सप्रे संग्रहालय में पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर के प्रयासों से संग्रहीत हैं, जो बताती हैं कि विपरीत माहौल में भी हिन्दी कैसे फली-फूली। आज भी हिन्दी पत्रकारिता खास तौर पर प्रिंट की अपनी शक्ति बरकरार है।
गांधी जी ने 1945 में हरिजन में लिखा था कि अखबारों में जो कुछ छपता है, उसे लोग ईश्वरीय सत्य मान लेते हैं। इस नाते संपादकों और अन्य पत्रकारों का दायित्व बढ़ जाता है। संचार और सूचना क्रांति के दौर में भी प्रिंट का महत्त्व इस कारण बरकरार है कि सदियों से छपे शब्दों की विश्वसनीयता लोगों के दिलोदिमाग पर मनोवैज्ञानिक रूप से छाई है। शब्दों का सौंदर्य विचारों का विस्तार, फत्रकारिता की गंभीरता, अभिव्यक्ति की मर्याद बाकी माध्यमों की तुलना में अखबारों के पन्नों पर कहीं अधिक प्रभावी रूप में दिखती है। खबरों की व्यापकता और सत्यता के लिए वे अगले दिन के अखबार का इंतजार करते हैं। वैसे तो प्रिंट मीडिया का इतिहास भारत में कलकत्ता से 1780 में निकले 'बंगाल गजट' से आरंभ होता है।
वह एशिया का अंग्रेजी का पहला साप्ताहिक अखबार था पर इसके संस्थापक हिक्की दो साल तक इसे चला नहीं सके और आंग्रेजों का कोपभाजन बने। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में छपने वाला मुंबई का पहला अखबार था, जिसका नाम बाद में 'बाम्बे टाइम्स' हुआ। बाद में तमाम अखबार छपे। 1821 में 'संवाद कौमुदी समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने निकाला।
1857 में हमारे पहले स्वाधीनता संग्राम में भी भाषाई अखबार संख्या में कम थे लेकिन बहादुरी से लड़े। उनको दबाने के लिए 13 जून, 1857 को लॉर्ड कैनिंग कुख्यात गैंगिंग एक्ट ताए। भारतीय भाषाओं के अखबारों को काबू में लाने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना। कई और कानून बने जिससे अखबारों को सताया गया पर सच लिखना जारी रहा। कई नायकों ने अखबार निकाले और डॉ. अंबेडकर भी उनमें से एक थे। 1943 में रानाडे की 101वीं जयंती पर उन्होंने बेबाकी से कहा था, 'आज पत्रकारिता का मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुन कर उसकी पूजा करना।
उसकी छत्रछाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी और विवेकसम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने ले लिया है, मुझे खुशी है कि कुछ सम्मानजनक अपवाद मौजूद हैं। आज भी स्थिति वही है। लेकिन सम्मानजनक अपवाद भी मौजूद हैं पर हिन्दी पत्रकारिता पर तमाम सवालों की बौछार हो रही है। हिन्दी पत्रकारिता में आज भी एकमत होकर मानक शब्दों पर सहमति तक नहीं बन सकी है। विश्व के तमाम नगरों और नेताओं के नाम हिन्दी अखबारों में एक जैसे नहीं छपते। हिन्दी में फराड़कर जी ऐसे संपादक रहे हैं, जिन्होंने इसके शब्द संसार को व्यापक बनाया। उन्होंने ही मिस्टर के लिए श्री, प्रेसीडेंट के लिए राष्ट्रपति जैसे शब्द दिए।
महामहिम, मुद्रास्फीति तथा कामचलाऊ सरकार जैसे शब्द उनके ही दिए हैं। सर्वश्री, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुरान, वातावरण, वायुमंडल, कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय, चालू, अंतरिम जैसे करीब 200 शब्दों में उनका योगदान माना जाता है। आम आदमी की भाषा की पैरोकारी के साथ उन्होंने जो प्रयोग हिन्दी पत्रकारिता में किए वे बंद हो गए पर ऐसा काम सीमित संपादकों ने किया और हाल के सालों में टीवी चैनलों ने अखबारों की भाषा भ्रष्ट करने का काम किया। हिन्दी पत्रकारिता और लेखन बड़े अर्थों में अनुवादजीवी या गूगलजीवी बन गई है। एआई उसमें एक नया आयाम है।
मिशन के साथ शुरू हिन्दी पत्रकारिता में खबर और विज्ञापन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। पेड न्यूज ने भाषाई अखबारों की छवि को आहत किया है। सरकारें पत्रकारों पर जब चाहे शिकंजा इस नाते कसती रहती हैं कि पत्रकारों को नियंत्रित करने के लिए 14 विभिन्न कानूनों का जाल है। हिन्दी भाषी इलाकों में साक्षरता बढ़ने के कारण बड़ा पाठक वर्ग, दर्शक और बोता पैदा हुआ है।
हिन्दी इलाका बड़ा बाजार भी है। अंग्रेजी, जिसे अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का गौरव है, के मूल शब्द मात्र 10 हजार हैं, लेकिन हिन्दी की शब्द संपदा ढ़ाई लाख से ज्यादा है। तमाम विसंगतियां हैं, फिर भी भरोसेमंद पत्रकारिता हिन्दी में अभी भी हो रही है। हिन्दी पत्रकारिता का सफर करीब 200 सालों का हो गया है। अब सूचना और संचार क्रांति के इस दौर को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया आयाम देने जा रहा है। इसका सृजनात्मक क्षमता और कल्पनाशीलता पर असर पड़ सकता है। हम मशीन पर निर्भर होते हुए अपनी स्वाभाविक बुद्धि और कौशल न खो दें, इस पर गंभीर चिंतन करने का समय है। तमाम मोस्चों पर हिन्दी को काम करने की जरूरत है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।


